Viram Chinh in Hindi Grammar Class 8
| Class | Class 8 |
| Subject | Hindi Grammar |
| Chapter | Viram Chinh |
Viram Chinh in Hindi Class 8
विराम चिह्न
विराम चिह्न का अर्थ है – रुकना, विश्राम करना या ठहरना होता |
भाषा के लिखित रूप में विशेष स्थानों पर रुकने का संकेत करने वाले चिह्नों को विराम-चिह्न कहते हैं |
विराम चिह्न के प्रकार
विराम चिह्न के प्रकार निम्नलिखित हैं|
- पूर्ण विराम ( | )
- अल्प विराम ( , )
- अर्द्ध विराम ( ; )
- प्रश्नवाचक चिह्न ( ? )
- विस्मयादिबोधक चिह्न ( ! )
- उद्धरण चिह्न ( ” ” )
- विवरण चिह्न ( :- )
- निर्देशक चिह्न ( ─ )
- योजक चिह्न ( – )
- कोष्ठक ( ) [ ]
- त्रुटिपूर्ण चिह्न ( ^ )
- लाघव चिह्न ( ० )
पूर्ण विराम ( | )
→ पूर्णविराम चिह्न कथन की पूर्णता का बोध कराता है |
जैसे – मेरा मित्र अध्यापक है |
मोहन पढ़ रहा है |
अर्द्ध विराम ( ; )
→ पूर्ण विराम से कुछ कम देर तक रुकने के लिए अर्द्धविराम का प्रयोग किया जाता है |
जैसे – खाना खा लो ; फिर चलेंगे |
बस्ता ले आओ ; बस आ गई |
अल्प विराम ( , )
→ वाक्य के अंदर अल्पकालीन विराम के लिए अल्पकालीन ( , ) चिह्न का प्रयोग सर्वाधिक होता है | इसका प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है |
→ जैसे → योजकहीन दो से अधिक सजातीय शब्दों के बीच में
→ (1) राधा, मोहन, ममता और शालू खेल रहे हैं |
→ वाक्य में जहाँ सबसे कम रुकना पड़ता है |
→ मैंने उस लड़की को देखा, जो पीड़ा से कराह रही थी |
विवरण चिह्न ( :- )
किसी कही हुई बात को स्पष्ट करने या उसका विवरण प्रस्तुत करने के लिए वाक्य के अंत में इसका प्रयोग होता है |
जैसे – (1) पुरुषार्थ चार है :-
धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष
निम्न :- संज्ञा, विशेषण
प्रश्नवाचक चिह्न ( ? )
प्रश्नवाचक वाक्य की समापित पर पूर्ण विराम का प्रयोग न करके, प्रश्नवाचक चिह्न ( ? ) का प्रयोग किया जाता है |
उदाहरण
- तुम्हारा क्या नाम है ?
- तुम क्या करते हो ?
- तुम कहाँ जा रहे हो ?
विस्मयादिबोधक चिह्न ( ! )
हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य आदि भाव प्रकट करने वाले शब्दों और वाक्यों के साथ विस्मयादिबोधक चिह्न (!) का प्रयोग किया जाता है |
उदाहरण
- अहा ! कितना अच्छा मौसम है |
- शाबाश ! तुमने बहुत अच्छा काम किया है |
उद्धरण चिह्न → (‘ ‘) (” “)
→ ये चिह्न दो प्रकार के होते हैं –
(1) दोहरे उद्धरण चिह्न (” “)
(2) इकहरे उद्धरण चिह्न (‘ ‘)
जब किसी व्यक्ति का कथन मूल रूप में लिखा जाता है, तब दोहरे उद्धरण चिह्न (“……”) का प्रयोग किया जाता है |
जैसे : “साहित्य समाज को दिशा प्रदान करता है”- डॉ. ब्रजकिशोर पाठक ने कहा |
पुस्तकों के नाम अथवा लेखकों के उपनाम इकहरे उद्धरण चिह्न में लिखे जाते हैं |
जैसे : ‘अभिज्ञान – शाकुंतलम’ महाकवि कालिदास की अमर रचना है |
सूर्यकांत त्रिपाठी ‘निराला’ महाकवि थे |
निर्देशक चिह्न (─)
→ नाटकों के संवाद में
जैसे – सीमा─बेटी, यदि तू जानती
कमलेश─क्या ?
→ समान कोटि की कई एक वस्तुओं का निर्देश किया जाय |
जैसे – काल तीन प्रकार के होते हैं –
भूतकाल, वर्तमानकाल, भविष्यत काल
→ जब कोई बात अचानक अधूरी छोड़ दी जाय |
जैसे – यदि आज माताजी जीवित होती ………… पर अब
→ जब वाक्य के भीतर कोई वाक्य लाया जाय
जैसे – महात्मा गाँधी─ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे─भारत की महान विभूति थे |
कोष्ठक ( )
→ कथाप्रसंग में किसी विशेष व्यक्ति की और संकेत करने के लिए |
जैसे – विभीषण (रावण के भाई) को घर का भेदी कहाँ जाता है |
→ नाटकादि में हाव-भाव सूचित करने के लिए किया जाता है |
जैसे –
प्रताप, तरुण से (क्रोधित होकर) झूठ बोलने का मज़ा अभी चखता हूँ |
वाक्य के बीच आए किसी शब्द का अर्थ बताने के लिए कोष्ठक (ङ) का प्रयोग किया जाता है; जैसे – तद्भव का शाब्दिक अर्थ – तत् + उससे + भव (उत्पन्न) |
वर्गीकृत विवरण में वर्गों की संख्या को कोष्ठक में रखा जाता है; जैसे – (अ) और (ब)
हंसपद या त्रुटिपूरक चिह्न ^
इस चिह्न का प्रयोग लिखते समय किसी शब्द या शब्दांश के छूट जाने पर किया जाता है और छूटे हुए शब्द या शब्दांश को ऊपर लिख दिया जाता है |
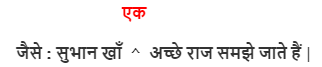
लाघव चिह्न o
शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए लाघव चिह्न का प्रयोग किया जाता है |
जैसे : अटल बिहारी वाजपेयी – अo बिo वाजपेयी
डॉक्टर – डॉo
बैचलर ऑफ़ आर्ट्स – बीo एo
भारतीय जनता पार्टी – बीo जेo पीo
योजक चिह्न (─)
(i) दो शब्दों को जोड़ने के लिए तथा द्वंद्व एवं तत्पुरुष समास में |
सुख─दुख, माता─पिता, प्रेम─सागर
(ii) पुनरुक्त शब्दों के बीच में |
पात─पात, डाल─डाल, धीरे─धीरे,
(iii) तुलनावाचक सा, सी, से के पहले |
भरत – सा भाई, यशोदा – सी माता
(iv) अक्षरों में लिखी जाने वाली संख्याओं और उनके अंशों के बीच जैसे एक – तिहाई, एक – चौथाई |
Hindi Vyakaran Class 8 Notes
- संज्ञा – संज्ञा के भेद
- सर्वनाम – सर्वनाम के भेद
- उपसर्ग – उपसर्ग के प्रकार
- कारक – कारक के भेद
- क्रिया ( अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया )
- काल और काल के भेद
- विशेषण और विशेषण के भेद
- वचन – वचन के भेद
- विराम चिह्न (Viram Chinh in Hindi Class 8)
- लिंग – लिंग के भेद
- मुहावरे और लोकोक्तियाँ
- प्रत्यय – प्रत्यय के प्रकार
- अव्यय (अविकारी)
- वर्तनी (Vartani)
- शब्द विचार (Shabd Vichar)
- शब्द भेद – अर्थ के आधार पर
- वाक्य – संबंधि अशुद्धिशोधन
- वाक्य रचना – वाक्य के भेद
- समास – समास के भेद (Samas or Samas ke bhed)
- संधि – संधि के भेद (Sandhi or Sandhi ke bhed)
- पद-परिचय (Pad Parichay in Hindi Vyakaran Class 10)
- अलंकार – अलंकार के भेद (Alankar or Alankar ke bhed)
- वाच्य – वाच्य के भेद (Vachya or Vachya ke bhed)
FAQs on Viram Chinh in Hindi Class 8
प्र.1. ‘विराम’ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है ?
उत्तर = रुकना या ठहरना
प्र.2. ‘कपड़े ले आओ पिताजी आ गए’ | उक्त वाक्य में अर्धविराम चिह्.न लगाकर बताइए –
उत्तर = कपड़े ले आओ ; पिताजी आ गए |
प्र.3. ( ) [ ] यह कौनसा चिह्.न है ?
उत्तर = कोष्ठक चिह्.न
प्र.4. जब किसी व्यक्ति का कथन मूल रूप में लिखा जाता है, तब किस चिह्.न का प्रयोग किया जाता है ?
उत्तर = उद्.धरण चिह्.न
प्र.5. ‘वाह क्या दृश्य है’ उक्त वाक्य में विस्मय सूचक चिह्.न लगाइए –
उत्तर = वाह ! क्या दृश्य है |
प्र.6. अध्यापिका – भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे ? उक्त वाक्य में प्रयुक्त इस चिह्.न (-) का नाम बताइए –
उत्तर = निर्देशक चिह्.न
1 thought on “Viram Chinh in Hindi Class 8”
Thank you so much